पूर्वोत्तर भारत: सांवरमल सांगानेरिया के यात्रा साहित्य के आइने में : प्रो. यशवंत सिंह
सच्चिदानंद हीरानंद
वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ स्वभावत: सैलानी व यायावरी प्रवृति
के लेखक थे। उन्होंने अपने यूरोपीय यात्रा-संस्मरण ‘एक
बूँद सहसा उछली’1 में लिखा है – ‘ज्ञान-वृद्दि
और अनुभव संचय के लिए देशाटन उपयोगी है … किन्तु देशाटन
कैसे किया जाय इसकी कोई विशेष पद्दति शास्त्रकारों ने नहीं बतायी-तीर्थादन की
परम्परा थी लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य
अनुभव-संचय नहीं
बल्कि पुण्य-संचय था
और वह भी भवानुभव से मुक्ति के लिए।’ घुमक्कड़प्रेमी और गाथाकार राहुल सांकृत्यायन ने ‘घुमक्कड़शास्त्र’2 नामक ग्रंथ का प्रणयन करके इस कमी को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने सम्पूर्ण भारत, तिब्बत, सोवियत रूस, यूरोप, श्रीलंका
इत्यादि देशों का भ्रमण करते हुए यात्रा से प्राप्त अनुभवों को इस यात्रा-वृत्तांत में
संजोया है, जो घुमक्कड़प्रेमियों
के लिए मार्ग-दर्शिका का
काम करता है। भारत देश में यात्रा, जो व्यक्ति के जीवन के अंतिम भाग में तीर्थयात्रा के रूप में सम्पन्न होती थी, उसको राहुल
जी ने व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन से जोड़ते हुए लिखा –
‘सैर कर दुनियाँ की गाफ़िल जिंदगानी फिर कहाँ?
जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ?’
हिंदी-साहित्य
की शुरुआत पूर्वोत्तर-भारत के वर्तमान असम-प्रदेश
से हुई, जहाँ पर
सिद्ध-साधकों ने ‘कामाख्याधाम’ से प्रचलित तंत्र-मंत्रप्रधान साधना
का प्रचार-प्रसार अपने
धार्मिक साहित्य के माध्यम से किया। फिर भी पूरे मध्यकालीन हिंदी-साहित्य में
पूर्वोत्तर-भारत की उपस्थिति नगण्य रही। असम के भक्तिकालीन महानसंत शंकरदेव जी ने ब्रजावली में बरगीतों की रचना करके इस कमी को दूर करने का प्रयास अवश्य किया। आधुनिककाल में अज्ञेय जी ने सम्भवत: पहलीबार पूर्वोत्तर-भारत को केन्द्र में रखते हुए अनेक कविताएँ, कहानियाँ और यात्रा-वृतांत रचे।
उनकी ‘पावस प्रात शिलङ्’ और ‘दूर्वाचल’ कविताएँ
मेघालय के रमणीय सौंदर्य को उजागर करतीं हैं। अज्ञेय की जयदोल, नीली हंसी, हीली-बोन की
बत्तखें, मेजर चौधरी की वापसी’ और नगा पर्वत की घटना आदि कहानियाँ पूर्वोत्तर-भारत के समाज को केन्द्र में रखकर रची गयीं हैं। अज्ञेय जी की जीवन-यात्राओं का
मुख्य उद्देश्य
अनुभव-संचय रहा
है। उन्होंने अपने पहले यात्रा-वृतांत – ‘अरे
यायावर रहेगा याद’3 में
पूर्वोत्तर भारत से सम्बन्धित तीन संस्मरण लिखे हैं। जिनमें से एक असम के सांस्कृतिक केन्द्र ‘माझुली-द्वीप’ की
यात्रा पर है, जिसके प्राकृतिक
सौंदर्य पर अज्ञेय का कवि-मन
मोहित हो जाता है। साथ ही, वहाँ के
निवासियों के रीतिरिवाज, वहाँ की प्रकृति, जंगली जानवर सब मनको आकर्षित करने वाले हैं। लेखक ने असम के निवासियों की मानसिकता और उनके स्वभाव के बारे में लिखा है – ‘असमिया लोग
खूब हँसते हैं, बाधाओं पर
और भी अधिक हँसते हैं। वह तो केवलकाम न करने की
एक युक्ति है और काम न करना पड़े
तो क्यों न हँसा जाये?’
पूर्वोत्तर-भारत
पर केन्द्रित यात्रा-वृतांत अथवा
यात्रा-कथा-लेखन की दृष्टि से सांवरमल सांगानेरिया का महत्तपूर्ण स्थान है। पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत असम प्रदेश के गुवाहाटी शहर में तीन अक्टूबर, 1945 ई. को मारवाड़ी
परिवार में जन्में सांगानेरिया जी के पूर्वज राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणपुर नामक गाँव से व्यापार के उद्देश्य
से असम आये थे। उन्होंने गुवाहाटी के कामर्स कॉलेज से ‘बी. कॉम’
तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से ‘कोविद’ की
उपाधि प्राप्त की। सन् 2012 ई. में जे.जे.टी.विश्वविद्यालय द्वारा
मानद ‘डी.लिट्’ की उपाधि प्राप्त डॉ. सांगानेरिया हिंदी
सहित असमिया, बाँग्ला और अंग्रेजी भाषाओं के भी जानकार हैं। अब तक उनके पाँच यात्रा-वृतांत/कथाएँ –
(१) थोड़ी यात्रा थोड़े कागज (1999 ई.), (२)
अरूणोदय की धरती पर (2010 ई.), (३)
ब्रहमपुत्र के किनारे किनारे (2015 ई.), (४)
फेनी के इसपार (2016 ई.) तथा
(५) मेघों के देस में (2020 ई.) प्रकाशित हो
चुके हैं। उनका पहला यात्रावृतांत – ‘थोड़ी यात्रा थोड़े कागज’4 भारत-यात्रा का
वृतांत है, जिसकी शुरूआत
गुवाहाटी शहर से होती है। लेखक की मान्यता है कि ‘यात्रा केवल
भौगोलिक रेखा पर चलना मात्र ही तो नहीं होती बल्कि इसमें इतिहास के पड़ाव भी होते हैं।’ यात्रा के दौरान आये इन्हीं ऐतिहासिक पड़ावों को जानना-समझना इनके
यात्रा-लेखन का
मुख्य उद्देश्य है।’
घुमक्कड़ी लेखक
के जीवन में कैसे समाई? इसकी खोजबीन करता लेखक अपने बालपन की स्मृतियों में खो जाता है। स्मृतियों पर छायी धुँध में लेखक को सर्वप्रथम सन् 1950 ई. में असम
में आया विनाशकारी भूकम्प याद आता है, जब पाँच-सात दिनों तक धरती रह-रहकर
डोलती रही थी। गुवाहाटी के फैंसी बाजार में असम की पारम्परिक शैली में लकड़ी से बने उनके दो-मंजिले
घर से ब्रह्मपुत्र नद
मुश्किल से पाँच-सात मिनिट
की पैदल दूरी पर ही प्रवाहमान है। घरवालों से छुपकर बचपन के हमजोलियों-संग ब्रह्मपुत्र
या फिर ‘दीघली पोखरी’ में नहाने जाना और जल-तरंगों
से अठखेलियाँ करना उस समय बहुत ही भला लगता था। प्रकृति के वैभव से इस तरह चुपके-चुपके लेखक
का परिचय होने लगा, वह इसकी
ओर आकर्षित होता गया। जो आगे चलकर लेखक की घुमक्कड़ी का आधार बनी। ‘दीघली पोखरी’ के बारे में यहाँ पर एक किंबदंती प्रचलित है कि ‘महाभारतकाल में
दुर्योधन की बारात की अगवानी के लिए यहाँ के राजा भगदत्त द्वारा इसे खुदवाया गया था।’ विदित हो
कि यहाँ के राजा भगदत्त की कन्या भानुमति का विवाह हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में राजा भगदत्त ने अपने जमाता दुर्योधन की तरफ से लड़ते हुए कुरुक्षेत्र में वीरगति प्राप्त की थी।
गुवाहाटी शहर
की अधिष्ठात्री देवी ‘कामाख्या’ हैं, जहाँ पर
माता सती का स्त्री-जननांग गिरा
था। नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर तक जाने का प्राचीन पैदल-पथ है।
इसे असुर नरकासुर ने एक रात्रि में बनाया था। नरकासुर मातेश्वरी कामाख्या के रूप पर मोहित हो गया था। अत: देवी ने
एक रात्रि में मंदिर तक पथ बनाकर पूर्ण करने की शर्त रखी। कुक्कुट द्वारा सूर्य उदय से पूर्व ही बाग देने से नरकासुर का प्रयास अधूरा रह गया। अब यह पथ, सड़क-मार्ग बन जाने से वीरान-सा हो
गया है। देवी कामख्या के भैरव उमानंद हैं, जो ब्रह्मपुत्र नद के एक टापू पर विराजमान हैं। पुराणकथा में ऐसा भी वर्णित है कि यहीं पर भगवान महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्मीभूत किया था। असुर नरकासुर ने अपनी माता ‘भूमि’ के नाम पर भौमा-वंश स्थापित
किया। अत्याचारी नरकासुर का भगवान श्रीकृष्ण ने लोककल्याण हेतु वध करके, उसके बेटे भगदत्त को प्राग्जोतिषपुर (असम का प्राचीन नाम) का राजा
बनाया था। पांडव भीम पुत्र घटोत्कच की ससुराल और उनके पुत्र वीर बर्बरीक की ननिहाल प्राग्जोतिषपुर ही थी। यहाँ के दैत्य मुर की वीरागंना पुत्री मौर्वी का पाणिग्रहण भीमपुत्र घटोत्कच से श्रीकृष्ण ने ही करवाया था। इन्हीं दोनों की संतान बर्बरीक ‘खाटू के श्याम’ नाम से विख्यात हैं, जिनकी कथा ‘महाभारत’ में वर्णित है। महाभारत युद्ध में राजा भगदत्त की वीरगति के बाद भौमा-वंश के
राजाओं ने यहाँ पर उन्नीस पीढ़ियों तक राज किया था।
‘अरुणोदय की धरती पर’5 लेखक का दूसरा यात्रावृतान्त है, जो पूर्वोत्तर
भारत के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा-कथा को
अभिव्यक्त करता है। हिमालय पर्वत के इसी प्रांगण में भारतमूमि पर सूरज की पहली किरण का प्रवेश होता है। यहीं पर प्राचीन समय में विदर्भ और चेदि राज्यों के स्थित होने की मान्यता मिलती है। यह केवल लोकविश्वास नहीं बल्कि इस बात के पुरातात्तिवक अवशेष भी यहाँ प्राचीन भीष्मक नगर में मिलते हैं। श्रीकृष्ण यहीं से रूक्मी और शिशुपाल को हराकर राजकुमारी रुक्मिणी का हरण करके द्वारका ले गये थे। पुराणकथाओं में वर्णित है कि किरात-वंशीय भीष्मक
कुण्डिलपुर का राजा था, जिसकी राजधानी
भीष्मक नगर थी। भीष्मक के रुक्मी आदि पाँच पुत्र और एक कन्या रुक्मिणी थी। भीष्मक नगर से दस-बारह
किमी. की दूरी पर कुण्डिलनगर जाने के रास्ते पर स्थित ताम्रेश्वरी देवी का मंदिर है; जिसे राजा
भीष्मक ने अपनी पुत्री रूक्मिणी की देवी-पूजा के
लिए बनवाया था तथा यहीं से श्रीकृष्ण रूक्मिणी का हरण करके ले गये थे। आज भी यहाँ के निवासी इदू मिश्मी अपना सम्बन्ध रूक्मिणी से मानते हैं। रूक्मिणी-हरण के
समय भ्राता रूक्मी ने श्रीकृष्ण से युद्ध किया था और पराजित हुआ था। तब श्रीकृष्ण ने रूक्मिणी के कहने पर अपने भावी साले रूक्मी को जीवनदान तो दे दिया किन्तु सजा के रूप में उसके बालकाटकर उसे अध-मुँडा
बना दिया। इसी पौराणिक घटना के स्मृति स्वरूप इदू मिश्मी जनजाति के लोग अपने बाल उसी तरीके से काटते हैं। लेखक के अनुसार – ‘हाँ, इस प्राचीन
परम्परा पर आधुनिकता का रंग जरुर चढ़ा है, जो स्वाभाविक
भी है।’
लेखक अपनी
यात्रा के दौरान जब परशुरामकुण्ड पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई कुण्ड या सरोवर नहीं बल्कि वह तो लोहित नदी है। जिसमें आगे चलकर किबांग नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ इसका ब्रह्मपुत्र नद
नाम से रुपांतरण हो जाता है। इसी नाम के कारण ब्रह्मपुत्र को
असमिया में लुइत, संस्कृत में लौहित्य और हिंदी में लोहित कहा जाता है। इसी जलधारा में परशुराम के हाथ से चिपका परशु छूटा था। उनकी पितृभक्ति भी बड़ी विकट थी, तभी तो
अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश पर उन्होंने अपनी माता रेणुका का सिर परशु से काट डाला था। लेकिन मातृ-हत्या के
पाप से वह परशु उनके हाथ में चिपक गया था। पुत्र की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर पिता ने उनसे वर माँगने को कहा तो परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित कर देने की प्रार्थना की। इससे उनकी माता को तो पुनर्जीवन मिल गया, फिर पिता
जमदग्नि के निर्देशानुसार ही परशुराम सह्याद्री (कोंकण) से चलकर इस ब्रह्मकुण्ड में
आये, जहाँ पर
लोहित-जल में
स्नान करने पर उनके हाथ से चिपका हुआ परशु छूटा, उन्हें मातृहत्या के दोष से मुक्ति मिली।
लेखक अपने
यात्रा-अनुभवों को
व्यक्त करते हुए लिखता है – पर्वतों-वनों-नदियों से हरा-भरा, तिब्बत (चीन) की सीमा
से लगा हुआ यह प्रदेश मिश्मी, आदी, निशी,
आपातानी, तागिन आदि विभिन्न जनजातियों की बहुरंगी संस्कृतियों का संगम है। इनके पारम्परिक पहनावे और त्योहारों पर होने वाले नृत्यों को देखना किसी के लिए भी कौतुक है। यहाँ के सेला दर्रे, तवांग, मायोदिया की बर्फीली वादियाँ किसी को भी रिझा सकतीं हैं। यहाँ के निवासी प्रारम्भ से प्रकृति-पूजक रहे
हैं, जो चाँद, सूरज, धरती, जल को ईश्वर मानकर अपने विधि-विधान से
पूजा करते हैं। यहाँ म्यांमार की सीमावर्ती खामति, सिम्फो, फकियाल आदि जनजातियाँ जहाँ हीनयान बौद्ध-धर्म की
अनुयायी हैं। वहीं तिब्बत (चीन) की सीमावर्ती
मोन्पा, शेरतुकपेन, मेम्बा, मेयोर आदि जनजातियाँ महायानी बौद्ध-धर्म अनुयायी
हैं। यहाँ के तवांग स्थित बौद्ध-गोन्पा और
उसमें विराजित छब्बीस फुट ऊँची भगवान बुद्ध की स्वर्णजड़ित मूर्ति के दर्शनकर अभिभूत हुए बिना रहा नहीं जाता। यहाँ की मेंगा शिव गुफा और हाल ही में जमीन के नीचे से निकले पच्चीसफुटऊँचे विशाल शिवलिंग को देखकर प्राचीन वैभव का अनुमान लगाया जा सकता है। सन् 1962 के भारत-चीन युद्ध
के समय चीनी सेना तवांग तक आयी थी लेकिन फिर वापस हो गयी थी। फिर भी चीन की गिद्ध दृष्टि इस सीमावर्ती प्रदेश पर हमेशा रहती है, जिसका प्रतिकार
यहाँ के निवासी अपनी प्रखर राष्ट्रभक्ति के द्वारा करते हैं।
बहुचर्चित ‘ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे’6 सांवरमल सांगानेरिया का तीसरा यात्रा-वृतांत है।
इस यात्रा में लेखक का मनोगत है कि ब्रह्मपुत्र और
असम दोनों एक-दूसरे
के पर्याय हैं। ब्रह्मपुत्र नद
के बिना असम की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मपुत्र ने
केवल असम का भूगोल ही नहीं रचा बल्कि असम के इतिहास को भी अपनी आँखों के आगे-से
गुजरते देखा है। इसकी घाटी में ही कामरूप, हैडम्ब, शोणितपुर, कौण्डिल्य, अहोम आदि कितने-ही राज्य
पनपे और बनते-संवरते रहे।
ब्रह्मपुत्र के
देखते- ही-देखते
सुदूर पूर्वी पटकाई दर्रा पारकर ब्रह्मदेश के
अहोमों ने इसकी घाटी में प्रवेश करके लगभग छह-सौ
वर्षों तक यहाँ शासन किया। ब्रह्मपुत्र घाटी
में पनपी सभ्यता ने ही विदेश से आये अहोमों को अपने रंग में रंगकर यहाँ की मिट्टी से
संस्कारित किया। इसी के किनारे जन्में
लाचित बरफुकन ने मुगल आक्रमणकारियों को मुँहतोड़ जबाब देकर उन्हें असम की सीमा से बाहर खदेड़ा था। इसके किनारों ने वर्मीज आक्रमणकारियों को खदेड़ने के बहाने घुस आये ब्रिटिशों के नृशंस अत्याचार देखे हैं। 15 अगस्त, 1947 ईं को देश को मिली स्वतंत्रता के नाम पर अपने शरीर को दो देशों की सीमाओं में बटने का दर्द भी ब्रह्मपुत्र ने
सहा है। यही तो है जो देश के इस भूखण्ड के प्रति बरती गई उपेक्षा को विभाजन के समय से देखता आया है।
ब्रह्मपुत्र-घाटी की तासीर ही थी कि श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव, दामोदरदेव जैसे अनेक महान संत यहाँ पर हुए। असम के श्रीमंत शंकरदेव (जन्म 1449 ई.) द्वारा प्रचारित
निराकारी पंथ ‘भागवती वैष्णव
धर्म’ के एक मात्र आराध्य ‘परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण’ हैं। उनके द्वारा चलाया हुआ वैष्णव मत ‘एक शरण धर्म’ यहाँ की लोकभाषा में ‘महापुरुषिया धर्म’ के नाम से विख्यात है। उन्होंने असम में नव-वैष्णवोत्थान
का नेतृत्तव किया, जिसमें ज्ञान और ध्यान के बदले भक्तिमार्ग को ही एकमात्र साधन-मार्ग बनाया
गया। इस मत को माननेवाले एक ऊँचे सुसज्जित आसन पर असमिया श्रीमद्भागवत को
देवतुल्य स्थापित कर उसके सामने भागवत-पाठ और
सामूहिक रूप से हरि-कीर्तन
करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि उनके समकालीन पंजाब के गुरु नानकदेव ने भी इन्हीं की तरह मूर्ति-पूजा का
निषेध करते हुए निराकार सिखपंथ चलाया था, जिसमें ‘गुरु
ग्रंथ साहब’ को सर्वोपरि आसन मिला हुआ है। विदित हो कि गुरु नानकदेव श्रीमंत शंकरदेव के जन्म से बीस वर्ष बाद सन् 1469 ई. में जन्में
थे तथा दोनों महापुरुषों का मिलन असम के ‘घुबड़ी’ नामक
स्थान पर हुआ था। यहाँ पर प्रसिद्ध गुरूद्वारा ‘दमदमासाहिब’ स्थित है, जहाँ गुरू
नानकदेव और गुरु तेगबहादुर स्वयं पधारे थे।
ब्रह्मपुत्र
नद के बीचोंबीच स्थित माझुली द्वीप में शंकरदेव जी को माधवदेव जैसे सुयोग्य शिष्य की प्राप्ति हुई, जो पहले
कट्टर
शाक्त-धर्मी कायस्थ
थे। एकबार उन्होंने देवी जी को बकरे की बलि देने की मनौती की और अपने बहनोई गयापाणि को इसकी व्यवस्था करने को कहा। गयापाणि शंकरदेव की शरण लेकर वैष्णव बन गये थे, अत:
उन्होंने बलि-प्रथा
का विरोध किया। इस पर दोनों में बहस छिड़ गयी, जिसपर दुखी
होकर गयापाणि ने कहा – ‘तुम मुझसे
बढ़-चढ़कर
वाद-विवाद
करने के बदले शंकरदेव से करो तो तुम्हारी बोलती बंद हो जायेगी।’ माधवदेव भी शास्त्र-पुराणों के
ज्ञाता थे, वे आवेश
में आकर शंकरदेव से बहस करने माझुली चल पड़े। लेकिन शंकरदेव के समक्ष पहुँचकर उनकी सौम्य-मूर्ति देखकर
वे अभिभूत हो गये और उन्हें प्रणाम किया। दोनों में काफी देर तक शास्त्रार्थ चला, अन्तत: गुरु
को अपने भावी शिष्य की प्राप्ति हो गयी।
श्रीमंत शंकरदेव
लोकधर्मी धर्मगुरु होने के साथ ही, बहुमुखी साहित्यिक
प्रतिभा के धनी भी थे। उन्होंने ब्रजभाषा और असमिया के साथ मैथिली का समावेश करते हुए ‘ब्रजावली’ को
प्रचलित किया। ब्रजावली में रचे हुए उनके बहुत-से पद ‘बरगीत’ के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसमें उनके
सुयोग्य शिष्य माधवदेव रचित गीतों का भी समावेश है। उन्होंने ‘अंकीया नाटकर गीत’ तथा
‘भटिमा’ (भाटों-चारणों द्वारा
गाये जाने वाले गीत) भी लिखे।
असम में ‘अंकीया’ नाट्य
विधा को प्रचलित किया तथा इसके लिए पत्नी प्रसाद, रुक्मिणी हरण, कालियदमन, केलि
गोपाल, पारिजात हरण, रामविजय आदि
छह एकसत्रीय नाटकों की रचना ब्रजावली में की। उनके द्वारा रचित तीन प्रबंधकाव्य-हरिश्चंद्र उपाख्यान, रुक्मिणी हरण और उरेषा (उड़ीसा) प्राप्त होते हैं तथा समूह गीतकाव्य विधा के अंतर्गत ‘कीर्तन घोषा’ नामक सर्वश्रेष्ठ कृति को उन्होंने सृजित किया। गरुड़ पुराण पर आधारित तत्त्व-दर्शन सम्बन्धी
काव्य – ‘भक्ति प्रदीप’ तथा श्रीमद्भागवत पुराण
के संक्षिप्त-सार-रूप को, एक दिन
में लिखकर ‘गुणमाला’ के रूप में प्रस्तुत करना भी उनके कृतित्त्व में शुमार है।
ब्रह्मपुत्र
के किनारों पर बसंत का आगमन ‘बिहू गीतों’ के साथ होता है। यहाँ पर निवास करने वाली बोड़ो, खासी, जयंतिया, गारो आदि जनजातियाँ अपनी-अपनी रंग-बिरंगी पोशाकों अपनी मान्यताओं, अपने रीति रिवाजों, आस्थाओं, अपनी बोलि-भाषाओं और
लोकनृत्यों से इस घाटी को अनुगुंजित करती रहती हैं। इस अवसर पर लेखक भावविभोर होकर मानो कह उठता है – ‘ॠतुराज बसंत
का लावण्य असमवासियों के चेहरों पर मानों चुहचुहा रहा है। नवपल्लवों की हरीतिमा गहरा गयी है। असमिया-बांग्ला नूतनवर्ष
प्रारम्भ होने में एक दिन-ही
रह गया है। … इसके साथ
ही मेरा मन-भी
हरहराया कि कितने ही वर्षों बाद मुझे रंङाली बिहू (रंगाली बिहू) पर असम में रहने का अवसर मिला है। इस समय प्रकृतिने नूतन परिधान धारण किया है तो फिर असमिया लोग बिनानवीन कपड़े पहने कैसे रह सकते हैं? यहाँ की
ग्रामीण स्त्रियाँ घर के करघों पर महीने-भर पहले
से ही बिहू पर बिहूवान के रूप में उपहार देने के लिए फुलाम गोमोछा (फूलदार गमछा), मेखला चादर आदि वस्त्र बुनने लगती हैं। बिहू पर आपसी आदान-प्रदान करने
के वस्त्रों को बिहूवान कहा जाता है, जिसमें अधिकतर
फुलाम गोमोछा ही दिये जाते हैं। सफेद सूत के गमछों पर लाल धागे से कलात्मक रूप में फूल तथा चौड़ी पाड़ (बार्डर) बुनी
जाती है। ये गमछे असमिया अस्मिता के प्रतीक हैं, जिन्हें भेंट
स्वरूप अर्पित करके किसी प्रिय या आदरणीय अतिथि का सत्कार भी किया जाता है। पर्व-त्योहारों पर
फुलाम गोमोछा का उत्तरीय गले में डालने का प्रचलन है। साथ ही, देव-देवियों के सिंहासन को सजाने के गमछों पर भगवान के नाम और चित्र भी बुने जाते हैं।
बिहू-उत्सव में असम के आदिम निवासी बोड़ो-कछारियों के
नीति-नियमों के
अनुसार-वनाच्छादित खुले
स्थान पर आबाल-बृद्ध, युवक-युवतियों का नर्तन होता है। गाँवों की अलग-अलग
बिहू-टोलियाँ होती
हैं, जिनमें खासी, जयन्तिया, चिम्फो, देउरी, मणिपुरी, लुशाई, भूटिया, अबोर, कुकी, नगा, मराण,
त्रिपुरी, मिरि (मिशिंग), लालुंग, कार्बी, डफला, नरा, टाई,
बोड़ो, कछारी, हाजोंग राभा आदि अविभाजित असम की सभी पर्वतीय एवं मैदानी जनजातियाँ अपने-अपने विशिष्ट
लोकनृत्यों, लोकवाद्यों और
लोकगीतों के साथ ब्रह्मपुत्र की
गाटी के मैदानी इलाकों में होने वाले बिहू-कार्यक्रमों में
सम्मिलित होतीं हैं। रंगाली-बिहू को
यदि रंगों का त्योहार कहें तो कोई अतिसयोक्ति न होगी। होली
में लगे रंगों को तो हम साबुन-पानी से
धोकर उतारते हैं, किन्तु बिहू
के रंग तो शाश्वत हैं। असमिया नारियों के तनपर सजे हुए रंग-बिरंगे
परिधानों को देखकर तो यही लगता है कि इन्होंने मूँगा, लाल, मोरपंखी, धवल, गुलाबी, नीला, हरा, हल्दिया अदि
भाँति-भाँति के
रंगों को ओढ़ रखा है। इस अवसर पर गाँवों-शहरों में
बच्चों तथा किशोर-किशोरियों की
टोलियाँ अपने कद के अनुरूप धोती और मेखला पहने ढोल और बाँस का टोका बजाते हुए घर-घर
जाकर नाचते-गाते हैं।
गृहस्थजन और दुकानदार आदि रूपयों-पैसों के
रूप में इन्हें बिहू की त्योहारी देते हैं।
सात-दिनोंतक मनाया जानेवाला यह बिहू-उत्सव अपने-आपमें अनेक विशेषताएँ लिए हुए हैं। आदिमकाल से मानव का सम्बंध कृषि-कार्यों से
रहा है, उसका आनंद-विषाद भी इन्हीं-से जुड़ा
है। हल-बैल
के बिना कृषि सम्भव नहीं थी, इससे यहाँ
पर एक कहावत प्रचलित हुई – ‘जार नाई
गोरू सि सबातो के खोरू’ अर्थात् जिसके पास गोधन नहीं वह सबसे क्षुद्र प्राणी है। इसीलिए बिहू-उत्सव का
प्रारम्भ गोरू-बिहू से
होता है। असमिया भाषा में गाय-बैल
को गोरू कहा जाता है। चैत्र-संक्रान्ति के
प्रभाव काल में कृषि की मूलाधार गायों को समीप के नदी-तालाब
में ले-जाकर
पिसी हुई उरद, हल्दी और
तेल आदि से मलकर नहलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। केले के पत्ते पर उनको विविध खाद्यान्न खिलाये जाते हैं और उनके लिए निरोगी रहने की कामना की जाती है। बिहू के अंतिम साँतवें दिन ‘कौड़ी-खेलना’ का प्रचलन है जिसका सम्बंध प्रजनन-शक्ति से
जोड़ा जाता है। इस खेल को साधारणत: बूढ़े-बूढ़ियाँ खेलते
हैं। इसी दिन कहीं हरिकीर्तन तो कहीं मैथेली-मेला लगता
है, जिसका सम्बंध
प्राचीनकाल में होनेवाली इंद्र-पूजा से
जोड़ते हैं। इस तरह गोरू-बिहू,
गोसाई-बिहू आदि
नामों से सात-दिन-तक बिहू-उत्सव मनाया
जाता है।
ब्रह्मपुत्र
नद असम प्रदेश के लिए जहाँ वरदान है, तो वहीं
उसके कुपित हो जाने पर बाढ़-सैलाब
के रूप में उसका विकराल तांड़व भी देखने को मिलता है, जो असम
के निवासियों का सर्वस्य हरण कर लेता है। इस नद के उत्तरीय पर माझुली, उमानंद जैसे द्वीपों के संग अनेक चापरियाँ भी बेल-बूटियों
की तरह टंकी हैं। इसके दलदली किनारे पर स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में एकसींगी गैड़ों ने अपने रमण-स्थल
बना रखे हैं, जो विविध
वन्यजीवों के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। यहाँ के बागानों में चाय की पत्ती खूब उपजती है, जिसके लिए
शिवसागर व डिब्रूगढ़ के
चाय-बागान
देश-विदेश
में विख्यात हैं। कहते है कि यहाँ पर निवास करने वाली सिंग्फों जनजाति पहले बीमारी को दूर करने के लिए इन पत्तियों को उबालकर पीती थी। बाद में लोकनायक मनीराम दीवान ने इन पत्तियों का परिचय अंग्रेजों को करवाया, जिससे यहाँ पर चाय का उत्पादन शुरू हुआ। अन्तत: ब्रह्मपुत्र की
घाटी तो ऐसी शस्य-श्यामला है
कि जो भी यहाँ आता है, वह यहीं
का होकर रह जाता है।
‘फेनी के इस पार’7 लेखक का चौथा यात्रा-वृतांत है
जो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा-प्रदेश की
यात्रा-कथा है।
त्रिपुरा भारत के भौगोलिक मानचित्र पर एक बिन्दु जैसा, बांग्लादेश के अंदर घुसा-हुआ दिखायी
देता है। यह प्रदेश अपने भू-भाग
का 84 प्रतिशत बांग्लादेश
से घिरा हुआ है, शेष 16 प्रतिशत भू-भाग
की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। देश विभाजन से पहले यह प्रदेश रेलमार्ग से असम के गुवाहाटी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ आदि और बंगाल के चटगाँव, ढाका, कोलकाता आदि शहरों से जुड़ा हुआ था। कसबा, अखौरा, फेनी आदि त्रिपुरा के निकटवर्ती रेलवे-स्टेशन हुआ
करते थे। लेकिन देशविभाजन के बाद त्रिपुरा का यह रेलपथ और वे सारे रेलवे-स्टेशन पूर्वी
पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में चले गये। वर्तमान में इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि असम के गुवाहाटी शहर से भी यह बहुत दूर लगता है और यहाँ तक पहुचना बहुत-ही श्रमसाध्य
या फिर वायुमार्ग से मंहगा है। वैसे ही पूरा पूर्वोत्तर-भारत, भारत की जनता से एक मानसिक दूरी पर है। फिर त्रिपुरा तो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए भी पास होकर दूर ही है।
भूतपूर्व राजवंशीय
त्रिपुरा प्रदेश अपने इतिहास के विभिन्न आयामों को समेटे और यहाँ की भिन्न-भिन्न जनजातीय
संस्कृतियों को अपने में समाहित किये हुए है। यह एक ऐतिहासिक सच है कि यहाँ की जनजातियों का पुराने समय से बंगाली हिंदुओं के साथ मेलजोल रहा है। यहाँ की त्रिपुरी, जमातिया, रियाङ्, नोयतिया, कलइ, रूपिनी, मुड़ासिंग, हालम और उचर जनजातियों में आचार-विचार और
परम्पराओं की थोड़ी-बहुत भिन्नता
रहते हुए भी इन्हें कोक्बोरोक भाषा
ने एक डोर में बांध रखा है। लेखक का आत्मकथन है कि ‘जब मैं
त्रिपुरा पहुँचा तो इसका एक-एक
पृष्ठ मेरी आँखों के सामने फड़फड़ाने लगा। यहाँ पर बांग्ला भाषा-संस्कृति का
ज्यादा प्रभाव है। एक तरह से देखा जाय तो इसे दूसरा बंगाल ही कहा जा सकता है।’ जो यहाँ
की जीवन-पद्धति में
साफ झलकता है।
पौराणिक कथानुसार
चंद्रवंशी राजा पुरुरवा के वंशज नहुष के पुत्र ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने से जब उनके चार पुत्रों ने मनाकर दिया, तब पाँचवें पुत्र पुरू ने पिता का बुढ़ाया स्वीकार किया। फलत: ययाति ने
उन चारों पुत्रों को अपने राज्य से निष्काषित कर दिया। जिससे उनके निष्काषित पुत्र द्रुह्यु ने
दक्षिण-पूर्व दिशा
में गंगा सागर (बंगाल की खाड़ी) के तट पर स्थित कपिलाश्रम क्षेत्र में आकर अपना प्रथक राज्य स्थापित किया। उन्हीं के वंशज प्रतर्दन ने वहाँ से बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र और
कपिली नदी क्षेत्र से आगे त्रिगर्त (वर्तमान त्रिपुरा) तक अपने राज्य का विस्तार किया। इन्हीं के वंशज चित्रायुध, युठिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में
सम्मिलित होने इंद्रप्रस्थ गये थे, जिनके महाप्रतापी
पौत्र त्रिपुर के नाम पर त्रिगर्त का नाम त्रिपुरा पड़ा। प्राचीन त्रिपुरा राज्य के मूल-निवासी
किरातवंशी ही थे। बांग्लादेश के वर्तमान सिलहट, कुमिल्ला, नोआखली और चटगाँव आदि स्थान इस राज्य के अंतर्गत सम्मिलित थे।
भारतवर्ष की
इक्यावन शक्तिपीठों में से एक ‘त्रिपुरेश्वरी – पीठ’
यहीं पर है। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र जलमहल – ‘नीरमहल’, विशालकाय श्वेत – ‘उज्जयंतप्रासाद’ और ‘पुष्पवंत-प्रासाद’ भी यहीं है। यहाँ जम्पुई पहाड़ की वादियों में मिजो लोगों को देखकर एक नया अनुभव होता है। ‘उनाकोटी’ में
बिखरा हुआ प्रस्तरशिल्प नवआंगतुकों के मन को लुभाता है। चारों ओर से छूतीबांग्लादेश की सीमाओं पर जाकर देश के हुए कृत्रिम बंटवारे का दुख मन को झिंझोड़ता है, सालता है।
त्रिपुरा के दक्षिणी छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर फेनी नदी के किनारे ‘सबरूम’ बसा है, फेनी नदी
यहाँ की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। फेनी नदी के इस पार खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि उस पार के बीस-पच्चीस
किलोमीटर का बंगोप सागर तट मानो हमें अपनी ओर आने का मौन आमंत्रण दे रहा है। यहाँ की त्रिपुरी, जमातिया, चकमा, रियाङ् आदि जनजातियों में काफी पढ़े-लिखेलोग
हैं, जिनमें कई
उच्चस्थ सरकारी पदों पर आसीन हैं। यहाँ पर निवास करने वालीं जनजातियों की बहुरंगी लोकसंस्कृति किसी-भी पर्यटक
का मन मोह लेती है।
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस राज्य की सातबार यात्राएँ कीं तथा यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपनी कालजयी रचनाएँ ‘राजर्षि’ (उपन्यास) व ‘विसर्जन’ (नाटक) लिखकर त्रिपुरा को विश्व-साहित्य में अमर बना दिया। त्रिपुरा राजवंश के महाराजा राधाकिशोर माणिक्य ने ‘शांतिनिकेतन’ की स्थापना में अहम् भूमिका निभाई तथा त्रिपुरा राजघराने की चार पीढ़ियों से गुरुदेव का आत्मिक सम्बंध रहा। यहीं की सौधी मिट्टी में सचिनदेव बर्मन जैसे महान संगीतकार का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। यह भी सच है कि इस प्रदेश ने पिछले कईवर्षों तक आतंकवाद का दंश सहा है। जिसमें हजारों बेगुनाह-निरोह लोग उस आतंकवाद की भेंट चढ़ गये। साथ ही, इस प्रदेश की प्रगति में भी आतंकवाद कई वर्षों तक रुकावट बना रहा। त्रिपुरा के लोगों के मन में, जीवन में, आतंकवादी दौर के वे दहशत-भरे दिन एक बुरे सपने की तरह आज भी मौजूद हैं।
‘मेघों के देस में’8 लेखक का पाँचवाँ व अब तक अन्तिम यात्रा-वृतान्त है, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के मेघालय प्रदेश की यात्रा-कथा को वर्णित किया है। ‘मेघों का आलय’ अर्थात् मेघालय पूर्वोत्तर भारत का प्राक्रतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एक बेहद-ही खूबसूरत और नयनाभिराम प्रदेश है, जहाँ पर मेघ हर कदम पर पाँव-चूमते हैं। यह प्रदेश अनेक ज्ञात, अज्ञात या अल्पज्ञात जनजातियों, यथा-खासी, जयंतिया और गारो का निवास-स्थान है, जो अपने विशिष्ट रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान, रंग-रूप के साथ ही भाषा, जीवन शैलीऔर धार्मिक विश्वासों के कारण अलग पहचान रखता है। पुराने जमाने से मेघालय में बसने वाली जनजातियों का दक्षिण में पूर्वी बंगाल (आज का बांग्लादेश) और उत्तर में असम से व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। ब्रिटिशों के आधिपत्य में आए असम और पहले से उनके अधीनस्थ बंगाल के मध्य खासी-पहाड़ एक सुदृढ़ दीवार की भाँति खड़ा था। अत: दोनों ब्रिटिश शासित प्रांतों को जोड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारी डेविट स्काट ने छल-कपट का सहारा लेकर और निरीह खासियों का खून-बहाकर सन् 1833 ई. में एक रास्ता बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्षों बाद ‘असम पुनर्गठन मेघालय एकट 1969’ के माध्यम से 24 दिसम्बर, 1969 को असम से अलग होकर मेघालय प्रदेश बना। जबकि 21 जनवरी, 1972 ई. को इसे पूर्णराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें असम के गारो, जयंतिया और खासी जिले सम्मिलित किये गये। इस प्रदेश की राजधानी शिलांग तक गुवाहाटी से सड़क-मार्ग द्वारा पहुँचना बहुत-ही आसान है, जबकि अभी हाल-ही में यह प्रदेश वायु-मार्ग से भी जुड़ गया है।
मेघालय में
निवास करने वाली खासी-जनजाति के
लोगों की मान्यता है कि शल्लोङ् देव ने अपनी पुत्री‘का-पाह्-संतीऊ’ को स्वर्ग से धरती पर भेजा, जिसकी संतानें ही खासी जनजाति के लोग हैं। इन्हें खासी अपनी आदिमाता मानते हैं, इससे इनमें
एक कहावत प्रचलित हुई – ‘‘लौंगएङ् ना
का किंथेइ’अर्थात् स्त्री
से ही इनकी जाति बनी है। तभी तो खासी-जयंतिया जनजातियों
का समाज मातृसत्तात्मक है, जहाँ पर
स्त्री का ही वर्चस्व होता है। पुरुष की विवाह-पूर्व कमाई
पर मातृ-परिवार और
विवाहेतर आय पर पत्नी का हक होता है। पति अपनी माँ-बहन
को चाहे भले कोई राय दे, परन्तु अपनी
पत्नी व बच्चों को
नहीं दे सकता। सम्पत्ति और घर की स्वामिनी पत्नी-ही होती
है। विवाहोपरांत पति ससुराल में रहता है, एक-दो बच्चे हो जानेपर ही वह चाहे तो अलग रह सकता है, लेकिन उसके
बच्चों का वंश माता के नाम से ही चलता है। माता की मृत्यु के बाद उसकी उत्तराधिकारी सबसे छोटी बेटी होती है, जो अन्य
बहनों को संकट आने पर अपनी सम्पत्ति का कुछ हिस्सा दे सकती है। खासियों में व्यवसाय आदि बाहरी काम स्त्री के जिम्मे होते हैं, जबकि घर
का कामकाज पुरुष के जिम्मे होता है। पुत्र होने पर घर के कामकाज में वह पिता की सहायता करता है, जबकि पुत्रियाँ
अपनी माँ के साथ रहकर दुनियादारी और व्यापार करना सीखतीं हैं। खासी-पहाड़ की
दक्षिणी ढलान पर स्थित चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए विख्यात रहा है, जहाँ पर
वर्ष में 500 से 700 इंच वृष्टि होती है। किन्तु वर्तमान में चेरापूंजी के पश्चिम में स्थित मावसीराम इसका स्थान ले रहा है।
शिलांग से
जयंतिया पहाड़ की ओर जाते हुए रास्ते में बहुतसी जगहों पर चपटे शिला-फलकों को
मैदान में खड़े देखा जा सकता है, जिन्हें ‘मावबन्ना’ अर्थात् स्मृति-स्तंभ कहा
जाता है। जयंतिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों अथवा किसी विशेष घटना की स्मृति में स्तंभों को जमीन पर खड़ा गाड़ते हैं। इन गाड़े हुए पत्थर के स्तभों के प्रति उनके मनमें बड़ी श्रद्धा होती है। यहाँ के नार्तियांग में बाग-बगीचे
की जगह पत्थरों का बगीचा देखा जा सकता है, जिसे लोग ‘मावबन्ना-पार्क’ अर्थात्
स्मृति-उपवन कहते
हैं। जयंतिया-जनजाति में
देवी-पूजा की
प्राचीन परम्परा रही है। नार्तियांग में बने ‘जयंतेश्वरी-देवी
के मंदिर को देश के इक्यावन शक्तिपीठों में स्थान प्राप्त है। इस शक्तिपीठ का निर्माण जयंतिपुर के राजा यशमलिक ने करवाया था, जहाँ आज
भी दुर्गापूजा होती है। विदित हो कि जयंतेश्वरी देवी का मूल मंदिर नार्तियांग से लगभग सौ किलोमीटर दूर स्थित जयंतियापुर (आज के बांग्लादेश) में है, जिसका यह
प्रतिरूप है। देश-विभाजन
के समय जयंतिया राज्य का कुछ भाग भी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, जिसके कारण
यह शक्तिपीठ विस्थापित हुई थी। प्राचीन जयंतिया राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी नार्तियांग थी, यहाँ पर
निवास के समय पूजा-अर्चना की
सुविधा हेतु राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जयंतिया जनजाति की इष्टदेवी जयंतेश्वरी-देवी हैं, जिसके नाम
पर यहाँ की जनजाति जयंतिया कहलाई।
मेघालय के
खासी-जयंतिया पहाड़ों
से गारों-पहाड़ तक
पहुँचने के लिए काफी घुमाव-फिराव लिए
हुए ऊबड़-खाबड़
रास्ता है। सागरतल से 2135 फुट की
ऊँचाई पर बसा ‘तुरा’
गारों पहाड़ का सबसे बड़ा शहर है। जहाँ तक पहुँचने के लिए घनघोर जंगलों से गुजरना पड़ता है। यहाँ से आगे मानकाचार कसबा एकदम पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की सीमा से लगा हुआ है, जहाँ पर
दो-देशों
की अंतरराष्ट्रीय सीमा कुछ घरों को छूकर या बीच में से निकली हुई है। यहाँ पर प्रकृति-प्रेमी राभा-जनजाति के लोगों का निवास है। मानकाचार में एक देवी-मंदिर भी
है, जिसे स्थानीय
लोग कामाख्या-देवी मंदिर
मानते हैं। राभा-जनजाति को
पर्वतों के आसपास, नदियों के किनारे गाँव बसा कर रहना पसंद है। ऐसा भी जन-प्रवाद
है कि गारो-पहाड़ के
दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र
की सोमेश्वरी नदी की घाटी में ‘चे-बोंगे’ और ‘बोंगे-काटे’ नामक दो बहनें थीं। इनमें-से एक
बहन गारो जनजाति के लड़के से विवाह करके गारो बन गई और दूसरी बहन अपने-ही सम्बन्धी
भाई से शादी करके, समाज से प्रताड़ित होकर गारों-पहाड़ की
उत्तर दिशा में चली गई। इस दूसरी बहन की संतति आगे चलकर रंदानि राभा के नाम से जाने गये। राभा जनजाति के लोग प्राचीन समय से अनेक देव-देवियों
के साथ ‘रिछिदेउ-या-चारपाकक’ अर्थात् महादेव शिव को मुख्य देवता मानते आये हैं। रिछि देवता के द्वारा राभा लोगों को स्वर्गराज्य से धरती पर लाने के कारण इन्हें ‘राबा’ कहा गया और ऐसी मान्यता है कि यही राबा शब्द समय के साथ उच्चारण से परिवर्तित होकर राभा बन गया।
इस तरह
सांवरमल सांगानेरिया जीने अपने यात्रा-साहित्य लेखन
में मणिपुर-प्रदेश को
छोड़कर समूचे पूर्वोत्तर-भारत की झलक दिलखाने का भागीरथी प्रयास किया है। एक मारवाड़ी परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने लक्ष्मी जी का संधान करने की बजाय सरस्वती-पुत्र होना
श्रेयस्कर समझा तथा अपनी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक दृष्टि
से पूर्वोत्तर-भारत को जानने-समझने का
सराहनीय कार्य किया। अन्तत: वे अपनी पूर्वोत्तर-भारत की यात्रा-कथाओं का
समापन इस कथन से करते हैं – ‘मेघालय ही
नहीं, पूरे पूर्वोत्तर-भारत में देखने-समझने के
लिए बहुत कुछ है, परन्तु सब
कुछ देख पाना संभव नहीं। फिर-भी
जितना देखा-जाना वही
भी मेरी स्मृतियों में संजोए रखने के लिए कम नहीं।’ अगर हम विद्यानिवास मिश्र
जी के शब्दों में कहें तो जीवन-यात्रा कभी
पूरी नहीं होती, बल्कि वह पूरी होने की चाह में ही अधूरी रह जाती है और जीवन अपनी देहरी पर पुन: दस्तक देने
लगता है, एक नये
जीवन की चाह में, एक नयी
जीवन-यात्रा की
शुरूआत के लिए।
1.
एक
बूँद सहसा उछली, सच्चिदानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, छठा संस्करण-2008 ई.।
2. घुमक्कड़शास्त्र, राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, नई दिल्ली, संस्करण-2013 ई.।
3. अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय, राजकमल
प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015 ई.।
4. थोड़ी यात्रा थोड़े कागज, सांवरमल सांगानेरिया, हेरिटेज फाउण्डेशन, पल्टन बाजार, गुवाहाटी, प्रथम संस्करण-1999 ई.।
5. अरुणोदय की धरती पर, सांवरमल सांगानेरिया, हेरिटेज फाउण्डेशन, गुवाहाटी, प्रथम संस्करण-2010 ई.।
6. ब्रह्मपुत्र के
किनारे किनारे, सांवरमल सांगानेरिया भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली, पहला संस्करण-2015 ई.।
7. फेनी के इस पार, सांवरमल सांगानेरिया, बोधि प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण-अप्रैल, 2016 ई.।
8. मेघों के देस में, सांवरमल सांगानेरिया, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, पहला संस्करण-2020 ई.।
पडीफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
कङ्ला पत्रिका अब टेलीग्राम पर है। हमारे चैनल @kanglapatrika में शामिल होने के लिए यहां क्लिक करें और नवीनतम अपडेट के साथ अपडेट रहें










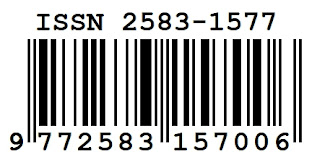

कोई टिप्पणी नहीं