आदिवासी स्वायत्तता और अस्मिता का सवाल : आदिवासी जीवन दर्शन का भविष्य : डॉ॰ जोराम यालाम नाबाम
रामदयाल मुंडा
अपनी पुस्तक ‘आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल’ में लिखते हैं, “भारतीय
संविधान में आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से एक विशिष्ट समुदाय माना गया है,
किन्तु उनकी कोई स्वतंत्र धार्मिक पहचान नहीं हैं । ” उन्होंने इस पुस्तक की
भूमिका में स्वीकार किया है कि आदिवासी लोगों ने अन्य ईसाई, मुसलमान या बौध
धार्मिक समुदायों में धर्मान्तरित होकर आंशिक रूप से अपने आदिवासीपन को खोया है,
तो उसका विकल्प हिन्दू बनना या बनाना भी नहीं हैं । आदिवासी प्रकृति पर विजय नहीं
पाना चाहते,बल्कि वे साथ
चलने के अनेक रास्ते खोजते रहते हैं । रामदयाल मुंडा ने‘आदि धर्म’ नामक पुस्तक में
मनुष्य और प्रकृति के बीच सह अस्तित्व, पारस्परिक निर्भरता को दिखाने का प्रयास
किया है ।
यह जान लेना
आवश्यक है कि ‘आदिवासी जीवन-दर्शन’ क्या है । आदिवासियों के लिए धर्म का क्या अर्थ
है ? वह किस तरह अन्य लोगों के धर्मों से भिन्न है ? धार्मिक राजनीति ने उसका क्या
नुकसान किया ? क्यों उस पर चर्चाएँ आवश्यक हैं ? बाहरी धर्मों के हस्तक्षेप ने किस
तरह सहज जीवन को असहज कर दिया है ? नई पीढ़ी किस तरह दो नाव पर कदम रखकर न आगे जा
पा रही है न पीछे लौट पा रही है और न ही बीच में सहज होकर खड़ी हो पा रही है ।
धर्म और दर्शन
जैसे शब्दों की व्याख्या न करते हुए मैं जिस समाज और समुदाय के परिवेश से आती हूँ
, अर्थात जहाँ हूँ, वहीं से एक उदाहरण उठाकर आपको बताने का प्रयास करूँगी कि धर्म और दर्शन
हमारे लिए क्या है ।
न्यीशी
अरुणाचल प्रदेश का एक बहुसंख्यक समुदाय है ।‘बुरिबूत’, ‘लुन्गते युल्लो’ और ‘न्योकुम
युल्लो’ हमारे प्रमुख त्यौहार हैं।‘लिमि पोल’ अर्थात फरवरी का यह महिना
न्योकुम-युल्लो का है। ‘न्योक’ का अर्थ है-जंगल, नदी, पहाड़, पशु-पक्षी इत्यादि और
‘कुम’ का अर्थ है एक साथ एकत्रित होना अथवा ‘एक होना’ । एक होने का यह भाव
स्नेह-अपनापन का अनुभव देता है , अत: इस स्थिति को ‘आने’ अर्थात माता माना गया । इसे
‘न्योकुम’ उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
हम मानते हैं
कि प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, न रात न दिन । समय का भी अस्तित्व नहीं था । इस स्थिति को ‘जिमी-जमा’ कहा गया । यह गर्भ है , यहीं से सब पैदा हो रहे हैं ;
तारे, नक्षत्र, धरती, आकाश सब । चाँद-सूरज उसी की आँखें हैं । इन्हीं आँखों से
धरती पर जीव और जगत का आगमन हुआ । दो प्राणी पैदा हुए-ऊई तानी अर्थात प्रकृति और
निया तानी अर्थात मनुष्य । ऊई तानी अग्रज , निया तानी अनुज है। इसीलिए अग्रज अनुज
की रक्षा करता है, अनुज चंचल हैं । दोनों के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। स्वभाव की
भिन्नता के कारण दोनों के बीच एक अप्रत्यक्ष ‘दापो’ अर्थात ‘सीमारेखा’ है । इस
‘दापो’ का अतिक्रमण वर्जित है ; नहीं तो संतुलन बिगड़ जाता है । इसका उल्लघंन आमतौर
पर अनुज अर्थात मनुष्य ही करता है , अत: अग्रज अर्थात प्रकृति उसे उसकी सजा देती
है ।
इस एक होने और
‘दापो’ अर्थात सीमारेखा का स्मरण करने के लिए न्योकुम मनाया जाता है । बड़ा भाई न्योकुम आने अर्थात प्रकृति माता के रूप
में आकर आशीर्वाद बरसाता है । इस दिन कौन मनुष्य, कौन जीव-जन्तु ; सब भेद को भुला
दिया जाता है । हम ही हैं सब । जब हम ही
सब हैं, तो गर्व का अनुभव होता है । इसी को
अभिव्यक्त करने के लिए कई कर्मकांड, गीत, मन्त्र इत्यादि मौजूद हैं ।इसी पर आधारित
है हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज और परम्पराएँ । सतुलन हमारा दर्शन है ।
आदिवासी दर्शन
की बात करते समय इसका खयाल रखा जाना चाहिए कि हमारे पास कोई लिखित धर्म और ग्रंथ
नहीं है। अभी तक हमने कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा। कोई शास्त्र नहीं लिखा। कोई
संगठित स्वरूप नहीं है। आप सोंचेंगे कि कोई धर्म नहीं है, कोई गुरु नहीं है, न
कोई गुरु शिष्य परंपरा। तो फिर यह समाज किस तरह से अनुशासित रहता होगा ? क्योंकि गैर
आदिवासी समाज का अनुभव कहता है कि इन्सानों ने धर्म की स्थापना इसलिए की कि समाज
में एक अनुशासन रहे और दुनिया उस अनुशासन के तहत सुचारु रूप से चलती रहे। उनकी
मान्यता के विपरीत हमारा कोई धर्म नहीं और न ही अनुशासित करने वाला कोई ग्रंथ - जैसा कि हिंदुओं में गीता,
मुस्लिमों में कुरान,ईसाइयों में बाइबल है।ईसाइयों में ‘टेन कोमाण्ड्मेंट्स’ यानी ईश्वर का दिया हुआ निर्देश
; जिसके अनुसार ईसाई धर्म के लोगों को चलना होता है। ऐसे ही अन्य धर्मों में भी
दिशा निर्देश हैं। हमारे पास इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं है। हम सिद्धांतों
में नहीं जिये अभी तक। हमारी जिंदगी
सिद्धांतों के निश्चित दायरे में बंधी हुई नहीं है। हमारी स्वतन्त्रता ही हमारा
मूलभूत सिद्धान्त है। यही कारण है कि धर्मान्तरण के बावजूद आदिवासी अपनी जड़ से अलग नही हो पा रहे हैं
। हमारी भाषा हमें अनुशासन देती है।
भारत के उत्तर-पूर्व की बात करें तो उनको अपने भिन्न दीखने
को लेकर भी रोज़ इस देश के लोगों के साथ जूझना पड़ता है। नाईजेरिया के महान लेखक चिनुआ
अचिबो ने अपने उपन्यास ‘द थिग्न्स फ़ॉल अपार्ट’ में नायक ओबो ओकोनक्वो द्वारा इसी
तरह के द्वंद्व को दिखाने का प्रयास किया है। नायक विदेशी शिक्षा के प्रभाव में
अपने रीति-रिवाजों से दूर हो जाता है।औपनिवेशिक जीवन शैली के कारण उसका दुखद अंत
हो जाता है। व्यक्ति न अपने प्रति, न अपने पारंपरिक ज्ञान संपदा के प्रति और न ही
अन्य समाज-संस्कृति के साथ ईमानदार हो पाता है। इसका एक उदाहरण अरुणाचल के सामजिक
जीवन में भी देखा जा सकता है ।हमारा दर्शन कहता है कि शराब अपने पूर्वजों से जुड़े
रहने का एक माध्यम है। यह उनके अनुभवों द्वारा संचित ज्ञान है । इसका सम्मान करना
चाहिए । इसलिए उन्हीं को याद करने के लिए पीओ । बेहोश होने के लिए नहीं पीना है । हमारे
पूर्वज हमें आतंकित नहीं करते, तो कई लोग भयमुक्त होकर पीने लगते हैं। इससे कई बार लड़ाई-झगड़े भी
हो जाते हैं। ईसायत ने कहा कि शराब पीना पाप है और उसकी सजा कौन तय करता है? उसे आदिवासियों
को समझाने के लिए कई-कई उदाहरणों, कथा-कहानियों का सहारा लिया गया। ईश्वर तथा उसके
बनाए नर्क नामक लोक से लोग आतंकित होने लगे । पीने वालों को शैतानी ताकत वाली आत्माओं
के रूप में माना जाने लगा । बहुत लोगों ने पीना छोड़ दिया। शराब की जगह पेप्सी,
कोका-कोला इत्यादि ने ले ली । विडम्बना यही है क्योंकि यह संतुलन में नहीं हैं।
इसके अलावा कई
रीति-रिवाज ऐसे हैं जिन्हें सबको निभाना ही होता है।यदि अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है तो उसे निभाना ही
होता है । पारंपरिक तरीकों से जब अपने पूर्वजों का स्मरण करना होता है तो शराब का
प्रयोग भी करना होगा। ऐसे में सामाजिक, सांस्कृतिक संतुलन बिगड़ने लगता है , व्यक्ति
मानसिक द्वंद्व से जूझने लगता है ।परन्तु हमें समझना होगा कि शराब ही क्यों, किसी भी समस्या अथवा बुराई को दूर करने के लिए शिक्षा
और वैज्ञानिक सोच का सहारा लिया जाना चाहिए।
रीति-रिवाज जीवन
को सहज और कवितामयी बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं । उसका पूर्णत: बहिष्कार ठीक नहीं हैं, और न ही यह
संभव है। भले ही हमारी आवाज बहुतों को सुनाई न दें पर इसका यह मतलब नहीं कि हमारी आवाज
दब गई है। वह किसी न किसी रूप में, पानी की तरह कहीं से भी अनायास प्रकट हो ही
जाती है। सदियों से आदिवासियों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहना
पड़ा है, आदिवासी फिर भी बचे रहे ।इसलिए आज
भी उनकी आवाज सुनायी दे रही है । इसका एक ही कारण है कि हम आधुनिक विकास की दृष्टि
से पिछड़े हो सकते हैं, किन्तु हमारी संस्कृति, दर्शन, इतिहास, रीति-रिवाज आदि बहुत समृद्ध है।ये
हमें संघर्ष के लिए ताकत देते हैं । हमारे भविष्य को भी इनसे इसी तरह ही ताकत मिलती रहेगी ।
जीवन दर्शन एक
व्यापक विषय है। ‘आदिवासी जीवन दर्शन’ कोई नया विषय नहीं है, भले ही
वह लिखित में कभी नहीं रहा, किन्तु इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी
हुआ कि लोगों ने उसे गहरे से धारण किया। उसे जीया। उसे जानने के लिए किसी किताब का
सहारा नहीं लिया। इससे व्यक्ति का अनुभव गहरा हुआ। हजारों सालों से यह चलता आ रहा
है। हमारे पूर्वजों द्वारा अपनायी गयी यह
रीति है; जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुँची है।
गैर आदिवासियों के लिए यह नया हो सकता है,
क्योंकि वे इससे अब तक अनभिज्ञ रहे हैं ।वे हमें सिर्फ कुछ किताबों और यात्रा वृत्तान्तों
के जरिये ही जान पाए हैं।
आदिवासियत कोई धर्म नहीं है। यह एक जीवन शैली है।
धर्म ग्रंथ के नाम पर हमारे पास प्रकृति है, जंगल है, सूरज है,
चाँद-तारे हैं, जमीन का हर एक टुकड़ा,
मिट्टी का एक-एक कण और कलकल बहती नदी ही हमारा धर्म ग्रंथ है। यह तो भारत संघ की
संरचना है, जो हमें जनगणना के समय धर्म के प्रकोष्ठ में कुछ
लिखना होता है। नहीं तो हमारी जीवन शैली ही हमारा दर्शन भी है और धर्म भी। हम धर्म
शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं करते, जिस अर्थ में शेष
भारत के लोग करते हैं। जिस तरह धर्म परिवर्तन हो रहा है उसे देखते हुए अब
आदिवासियों को भी अपना संगठित धर्म बनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी है । क्योंकि
इसके बिना अपनी संस्कृति को बचाना कठिन हो
गया है। इसी से एक तरह का संघर्ष देखने को मिलता है । धर्मों ने एक तरह का वैमनस्य
फैला रखा है । यदि अदिवासी भी इस श्रेणी में आ जाते हैं, तो
कहना मुश्किल है कि वास्तविक आदिवासियत बची रह सकेगी । आदमी शायद इसी तरह प्रकृति
से दूर होता जाता है ।
दुनिया में
जितने भी आदिवासी हैं, उनके रहन-सहन, आस्था-अनास्था, खानपान आदि में फर्क दिखायी
देता है। भाषाओं में, परम्पराओं में भी पर्याप्त भिन्नता है।
लेकिन इसके बावजूद हमारा दर्शन एक है। प्रकृति और पूर्वज ही हमारे धर्म का आधार है।यह
प्राकृतिक धर्म है । इस आधार पर दुनिया भर के आदिवासी एक ही धर्म का पालन करते हैं।
रामदयाल मुंडा ‘आदि धर्म’ के पृष्ठ 39 में पुजारी द्वारा गाये जाने वाले गीतों का अनुवाद करते हुए
लिखते हैं, “मनुष्य के अमरत्व में विश्वास करना । मृतक की आत्मा की छायारूप में घर
वापसी के अनुष्ठान में थोड़े-बहुत अंतर के साथ सभी आदिवासियों में संपन्न होता है ।
”
आदिवासियों का
सामजिक ढाँचा, न्याय इत्यादि की व्यवस्थाएँ भी प्रकृति के साथ संतुलन को ध्यान में
रखकर बनाया जाता है । जैसे, एक गाँव के लोग अपने आस-पास के जंगलों का संरक्षण जिस
तरह करते हैं । सभी का अपना-अपना जंगल होता है । पेड़ों की कटाई जब-तब नहीं कर सकते
। जितना जरूरत है उतना ही लो । कोई किसी के जंगल से पेड़ नहीं काट सकता,परन्तु लकड़ियाँ, सब्जी इत्यादि रोजमर्रा के
जरूरत को कोई भी किसी के भी जंगल से ले सकता है।
हम ऐसा मानते
हैं कि कोई भी चीज मृत नहीं है। सबमें
जीवन है। हमने एक पेड़ काटा लेकिन पेड़ जो
है वह कटने के बाद भी जीवित है। एक न्यीशी मुहावरा है- “सोपो यान बो हो तयिन नह
बुल्ले यादन्न ला”, अर्थात सड़ी हुई लकड़ी पर कुकुरमुत्ते ज्यादा उगते हैं। यदि वह मृत है तो फिर कुकुरमुत्ते उगे कैसे? उसपर काइयाँ या दूसरे पौधे उगते हैं ये
कहाँ से आए?झूम खेती एक बार जहाँ कर लिया, इसके बाद कुछ साल
उसे ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं ताकि जंगल को फिर से उगने का अवसर मिल जाए । शिकार
के भी अपने नियम होते हैं । कुछ वर्जित नियमों का पालन करना होता है । जंगल की
आत्माएँ नाराज अथवा प्रसन्न होती हैं, फायदे-नुकसान कुछ भी हो सकता है ।
इसी तरह की
आस्थाओं ने सदियों से मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन को बनाये रखने में बड़ी
भूमिका निभाई है । माँस खाना, शिकार करना इत्यादि पहले से अधिक हो गया है । जानवरों
का माँस हर सडक, हर गली में बिकते हुए पाया जाता है। यह आदिवासी जीवन शैली के
विपरीत है। हम विकास विरोधी नहीं हैं, परन्तु इस तरह के विनाशकारी विकास का हम
पुरजोर विरोध करते हैं। इस संबंध में डॉ.
गंगा सहाय मीणा की पुस्तक ‘आदिवासी चिंतन की भूमिका’ में लिखी पंक्तियों का स्मरण
हो आता है,“संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुझाया गया आदिवासियों के लिए आत्मनिर्णय का हक एक
बेहतर रास्ता हो सकता है, यानी विभिन्न राष्ट्रों के आदिवासियों को राज्य आत्मनिर्णय
का अधिकार दें । उन्हें शेष समाज से जोड़ने का काम करें। आदिवासी स्वयं निर्णय करें
कि वे कैसा विकास चाहते हैं । ”
किसी समाज
अथवा संस्कृति का अहं ज़िद्द पकड़ने लगे कि उसी की कल्पना श्रेष्ठ है;
यहीं से द्वंद्व का प्रारंभ हो जाता है ।इस द्वंद्व में
विजयता बनने के लिए किसी अन्य समाज की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना होता है,
उनकी संस्कृतियों पर अतिक्रमण आवश्यक हो जाता है,
और इस क्रम में भाषा, इतिहास और पहचान आदि मिट जाया करती है । इनके मिट जाने का
अर्थ है एक ज्ञान धारा का मिट जाना, एक सभ्यता का मिट जाना । इसके बाद क्या ?
संघर्ष तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता,! वह तो चलता ही रहता है मुझे लगता है भौतिक विकास
जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे लोग धीरे-धीरे जीवन को कल्पनाओं में जीने लगेंगे।चूँकि
जीवन कल्पना नहीं है, सत्य है । कल्पनाएँ अनेक अनावश्यक नियमों का निर्माण करने लगती हैं । यह
नियम कब मानवता के विरुद्ध खड़ा होने लग जाए इसका पता होते-होते अक्सर देर हो जाती
है। यह प्रकृति से दूर होने का परिणाम स्वरूप होगा । जिन मानव समुदायों को विकसित
कहे जाने वाले समाजों ने जंगली मानकर उपेक्षा की, वे तो
विज्ञान को वास्तव में दैनन्दिन जीवन में जीते हैं ।जो जितना प्रकृति के नजदीक
होगा, वह उतना ही वैज्ञानिक स्वभाव वाला होगा । इसको देखने
के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा । इनके करीब आना होगा ।
ग्रीक
दार्शनिक पाइथोगोरस ने जब ‘फिलोसोफी’ शब्द का इजाद किया होगा, उस वक्त उनकी मन:स्थिति गर्भ की ओर लौटने
की ही रही होगी।आदमी ने अनुशासन और नियम के नाम पर मकड़ियों का जाल बुन लिया है, जिसके चलते लौटना आसान होते हुए भी कठिन हो गया। प्रकृति के स्वतंत्र
सिद्धांत को फिर से समझने की आवश्यकता है । आदिवासियत इसी से बनी है। यह मानवता को
एक नई दिशा दे सकती है ।इसका संकुचित अर्थ देखना इसके प्रति अन्याय है। इसी को
ध्यान में रखते हुए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय जनगणना प्रपत्र में
आदिवासियों का नाम यानी उसकी असली पहचान को मान्यता दें, जिस तरह देश की आजादी के
पहले हुआ करता था ताकि हमें यह न लगे कि ब्रिटिश शासक ही असल में हमारे हितचिन्तक
थे ।
यदि
आदिवासियों की संख्या को अलग से दिखाने के लिए भारतीय जनगणना प्रपत्र में उनको ‘कोलम कोड’ दे दिया जाता है, तो सबकुछ स्पष्ट हो जायेगा;
क्योंकि सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दृष्टि से ये अपनी भिन्न पहचान रखते हैं। इससे
धर्म परिवर्तन खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, किन्तु संतुलन आवश्य आएगा । आदमी
अपनी पहचान के साथ रहना चाहेगा । हिन्दू तथा मुस्लिम को छोड़कर बाकी सभी धर्म और
संस्कृति वाले लोगों से आदिवासियों की संख्या अधिक है,इस दृष्टि से भी कोकोड की मांग जायज हैं ।
स्वतंत्रता के पूर्व जो‘
एनिमिस्ट (आदिवासी) नाम था, उसी को वापस जनगणना प्रपत्र में
डाल दिया जाना चाहिए।
भारतीय जनगणना
प्रपत्र
(द्वारा रजिस्ट्रार जनरल तथा सेंसेस कोमिशनर;
मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफियर भारत सरकार)
भारत की प्रथम
जनगणना 1871-72से लेकर 1941-42 तक आदिवासियों के लिए निम्नलिखित नाम शब्द को धर्म/कोलम कोड के लिए अंकित किया गया ;
-
सेंसेस ऑफ़ इंडिया;
‘झारखंड में
मेरे समकालीन’ के प्रणेता आदिवासी जीवन के अध्येता प्रोफेसर वीर भारत तलवार लिखते
हैं, “आदिवासियों का निश्चित रूप से अपना अलग धर्म है । उनके धर्म विशेष को ‘अन्य’
खाते में डाल देना उनका धार्मिक अपमान करना है । उनके अपने धर्म को जनगणना में
स्वीकार नहीं करना संस्थागत रूप से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार की अवहेलना करना
है और यह अवहेलना सरकार खुद कर रही है । ” स्वतन्त्रता के बाद वाले जनगणना में
आदिवासियों की पहचान स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ‘अन्य’ (एस.टी.) वाले खाते में अन्य
धर्म के लोग भी शामिल हैं-बौद्ध, हिन्दू, सिख, इसाई, पारसी इत्यादि । जिस दिन यह प्रावधान हट जाएगा उस दिन
आदिवासियों का अस्तित्व कहाँ होगा ? यह‘अन्य’
शब्द भ्रामक है। इसी के कारण आदिवासी अपनी पहचान को लेकर
भ्रमित रहते हैं । इस दिशा में गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए।
सहायक ग्रन्थ
:
1. द थिंग्स फ़ॉल अपार्ट - चिनुआ अचीबी
2. आदिवासी
चिंतन की भूमिका - गंगा सहाय मीणा
3. झारखंड
में मेरे समकालीन -वीर भारत तलवार
4. डीकोलोनिजिंग
द माइंड - न्गुगिवा थ्योंग्यो
5. आदि धर्म
- रामदयाल मुंडा
6.आदिवासीनामा
- डॉ. बनना राम मीणा
7. द
ऑक्सफ़ोर्ड इंडिया इल्विन - जे. एन. देवे
8. जसिनता
केरकेट्टा की कविताएँ
9. मराठी
कवि वाहरू सोनवणे की कविताएँ
10.आदिवासी
अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल- रामदयाल मुंडा
-----
संपर्क-सूत्र
:
हिन्दी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
ईमेल : 9436044288
मोबाइल : yalamnabam3@gmail.com
x








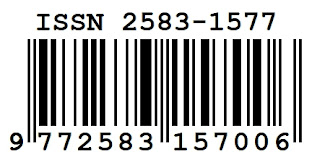

कोई टिप्पणी नहीं